भारत में सांस्कृतिक विकास
भारत में सांस्कृतिक विकास – जब तुर्क लोग भारत आए तो उनके पास न केवल एक सुपरिभाषित धर्म था , बल्कि शासन , कला , स्थापत्य आदि के संबंध में उनके अपने विशिष्ट दृष्टिकोण भी थे।
आरंभ में उन्होंने मंदिरों और दूसरी इमारतों को मस्जिदों में बदल दिया। इसके उदाहरण कुतुब मीनार के निकट कुव्वल – उल – इस्लाम मस्जिद और अजमेर का ‘ अढ़ाई दोनों का झोपड़ा ‘ नामक इमारतें हैं।
‘ कुब्वल – उल – इस्लाम मूल्यत : एक जैन मंदिर था जिसे बाद में वैष्णव मंदिर के रूप में बदल दिया गया था। ‘ अढ़ाई दिन का झोपड़ा ‘ एक मठ था।
दिल्ली की मस्जिद में बनवाये गये मेहराबों की सजावट के लिए जिस शैली का इस्तेमाल किया उनमें किसी भी मानव या पशु – पक्षी की आकृतियों का इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि ऐसा करना इस्लाम के खिलाफ होता। इसके बदले उनमें बेल – बूटों और कुरान की आयतों को एक दूसरे में अत्यंत कलात्मक ढंग से गूँथ दिया गया।
अपनी इमारतों में तुर्कों ने मेहराबों और गुंबदों का भरपूर प्रयोग किया। न तो मेहराबों की और न गुंबदों की ही ईजाद तुर्कों या मुसलमानों ने की थी। अरबों ने बैजंतिया साम्राज्य के जरिए उन्हें रोम से सीखकर उनका विकास करके अपना बना लिया था।
मेहराबों और गुंबद की जानकारी भारतीयों को भी थी लेकिन वे उनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर नहीं करते थे। भारत में सांस्कृतिक विकास
भारतीय सामान्यत: जिस युक्ति का प्रयोग करते थे वह यह थी कि वे एक पत्थर पर दूसरा पत्थर कुछ बाहर की ओर निकालकर इस तरह जोड़ते जाते थे कि बीच का अंतराल काम होता चला जाता था और अंत में जो थोड़ा अंतराल बच जाता उस पर ढक्कन के तौर पर एक पत्थर डाल देते थे या पत्थर की पटियों पर शहतीर डाल देते थे।
तुर्क शासको ने अपनी इमारतों में गुंबद और मेहराब पद्धति तथा लिंटल और शहतीर पद्धति दोनों का इस्तेमाल किया।
सजावट के मामलों में तुर्कों ने धार्मिक कारणों से मानव आकृतियों या पशु – पक्षियों की आकृतियों के इस्तेमाल से परहेज किया। इसकी बजाय वे ज्यामितिक और फूलों के डिजाइनों का प्रयोग करते थे और उन्हें कुरान की आयतों से बनाए गए चरख़ानों ( पेनल ) में कलात्मक रीती से मिला देते थे।
इन सजावटी युक्तियों के संयोग को अरेबेस्क कहा जाता था। उन्होंने घंटी , स्वस्तिक , कमल आदि हिन्दू प्रतीकों का भी निस्संकोच इस्तेमाल किया।
बलुई पत्थरों का इस्तेमाल करके तुर्कों ने अपनी इमारतों को अलग-अलग रंगों की छटा भी प्रदान की। इन इमारतों में सजावट के लिए पीले बलुई पत्थरों या संगमरमर का इस्तेमाल किया गया ताकि लाल बलुई पत्थरों का रंग निखर कर सामने आए। भारत में सांस्कृतिक विकास
तुर्कों द्वारा 13वीं सदी में किया गया सबसे शानदार निर्माण कुतुबमीनार थी। इस मीनार को दिल्ली के लोकप्रिय सूफी संत कुतुबमीनार बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाया गया था।
यह मीनार मूलतः 71.4 मीटर ऊँची है। लाल और सफेद बलुई पत्थरों तथा संगमरमर का इस्तेमाल और धारीदार छवि , ये इस मीनार की ऐसी विशेषताएं है जो खास तौर से प्रभावित करती है।
अलाउद्दीन ने अपनी राजधानी सीरी में काफी इमारतें बनवाई जो कुतुबमीनार के इलाके से कुछ किलोमीटर दूर पड़ता है।
अलाउद्दीन ने कुतुबमीनार से दुगनी ऊंची एक मीनार बनवाने की योजना बनाई लेकिन उसे पूरा करने के लिए जिंदा नहीं रहा। अलबत्ता कुतुबमीनार में उसने एक प्रवेश द्वार अवश्य जोड़ दिया।
अलाई दरवाजा के नाम से ज्ञात इस द्वार के मेहराब बहुत आकर्षक लगते हैं। इसमें एक गुंबद भी है जो वैज्ञानिक पद्धति से बनाया गया सही पहला गुंबद है।
तुगलक शासनकाल में , जो दिल्ली सल्तनत के चरमोत्कर्ष के साथ ही उसके पतंन की शुरुआत का भी काल था , भवन – निर्माण की गतिविधियों में बहुत तेजी आ गई। भारत में सांस्कृतिक विकास
गयासुद्दीन और मुहम्मद तुगलक ने तुगलकाबाद का विशाल किला बनवाया और यमुना के बहाव को रोककर उसके चारों ओर एक विशाल कृत्रिम झील बनवाई गई।
तुगलक स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता ढालू दीवार है। इससे इमारत के मजबूत और ठोस होने का एहसास होता है।
लेकिन फिरोज तुगलक की इमारतों में हमें ढालू दीवारें देखने को नहीं मिलती। फिरोज स्थापत्य कि एक अन्य विशेषता यह थी कि इसमें जानबूझ कर मेहराब तथा लिंटल – शहतीर सिद्धांतों के संयुक्त प्रयोग का प्रयत्न किया गया।
हौजखास में एक मंजिल में मेहराबों का इस्तेमाल किया गया है तो दूसरी में लिंटल – शहतीर पद्धति का। फिरोजशाह के नए किले में भी जो कोटला के नाम से प्रसिद्ध है , यह बात देखने को मिलती है।
तुगलक सुल्तानों ने अपनी इमारतों में आम तौर पर कीमती बलुई पत्थरों का इस्तेमाल नहीं किया। उसकी बजाय उन्होंने सस्ते और आसानी से उपलब्ध भूरे पत्थरों का प्रयोग किया। इस तरह के पत्थर में नक्काशी करना आसान नहीं है इसलिए तुगलक कालीन इमारतों में कम – से – कम सजावट दिखाई देती है। भारत में सांस्कृतिक विकास
फिरोज तुगलक की सभी इमारतों में सजावट के लिए कमल का इस्तेमाल किया गया है।
लोदियों की परंपरा में मेहराबों तथा लिंटल – शहतीरों दोनों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा गुजराती , राजस्थानी शैली के छज्जों , छतरियों और गुफाओं का भी इस्तेमाल हुआ है।
लोदियों ने जो एक और तरीका अपनाया वह यह था कि उन्होंने अपनी इमारतें , खासकर मकबरे , ऊंचे चबूतरों पर खड़ी की जिससे वे देखने में विशाल लगती हैं।
कुछ मकबरे बगीचों के बीच में बनवाए गए। दिल्ली का लोदी उद्यान इसका एक नमूना है। कुछ मकबरे अष्टभुजाकार थे।
इनमें से बहुत – सी विशेषताओं को बाद में मुगलों ने भी अपनाया और इनकी चरम परिणति शाहजहाँ द्वारा बनवाए गए ‘ ताजमहल ‘ के रूप में हुई।
तुगलकों द्वारा चौदहवी और पंद्रहवीं सदियों में दिल्ली में विकसित स्थापत्य शैली को विभिन्न राज्यों ने आगे बढ़ाया और उसमें परिवर्तन तथा सुधार किए। भारत में सांस्कृतिक विकास
धार्मिक विचार और विश्वास
जब तुर्कों ने उत्तर भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की उस समय इस्लाम भारत के लिए कोई अपरिचित धर्म नहीं था।
सिंध में आठवीं सदी से और पंजाब में दसवीं सदी से इस्लाम स्थापित था। आठवीं और दसवीं सदियों के बीच केरल में अरब व्यापारी बस गए थे।
सूफी आंदोलन के बारहवीं सदी के बाद भारत में अपनी जड़े जमाने के पश्चात इस आंदोलन ने मुसलमानों तथा हिंदुओं दोनों को प्रभावित किया।
दसवीं सदी में अब्बासी खिलाफत के ध्वंसावशेषों पर तुर्कों का उदय हुआ । इस सदी में मुताजिला या बुद्धिवादी दर्शन का बोलबाला खत्म हो गया तथा कुरान तथा हदीस ( मुहम्मद और उसके साथियों से संबंधित परंपराओं ) पर आधारित रूढ़िवादी विचार – धाराओं और सूफी रहस्यवादी पंथ का उदय हुआ।
इस्लामी कानून की चार धाराओं में से सबसे उदार हनीफी धारा थी और इसी को पूरबी तुर्कों ने अपनाया और यही तुर्क बाद में भारत आए।
सूफी कहे जाने वाले रहस्यवादियों का उदय इस्लाम में बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में ही हो चुका था। भारत में सांस्कृतिक विकास
कुछ सूफियों ने , जैसे महिला रहस्यवादिनी राबिया ( आठवीं सदी ) और रहस्यवादी मंसूर बिन हल्लाज ( दसवीं सदी ) ने ईश्वर और जीवात्मा को एक – दूसरे से जोड़ने वाले तत्व के रूप में प्रेम पर बहुत जोर दिया।
अल – गज्जाली ने ( मृत्यु : 1112 ई ) , जिसका आदर रूढ़िवादी और सूफी दोनों करते हैं , रहस्यवाद और इस्लामी रूढ़िवादिता में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की , और बहुत हद तक वह इस कोशिश में कामयाब भी रहा।
अल – गज्जाली ने ‘ बुद्धिवादी ‘ अल्ला और उसकी खूबियों की सच्ची अनुभूति बुद्धि से नहीं , बल्कि सिर्फ संबुद्धि यानी , इलहाम से ही प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार इलहामी ग्रंथ कुरान रहस्यवादियों के लिए सबसे महत्त्व की चीज थी।
इस समय के आसपास सूफी 12 पंथों या सिलसिलों में संगठित थे। हर सिलसिलें का नेतृत्व आम तौर पर एक प्रसिद्ध सूफी संत करता था जो पीर कहलाता था और अपने शिष्यों या मुरीदों के साथ खानकाह अर्थात आश्रम में रहता था।
पीर और मुरादों का संबंध सूफी धर्मव्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग था। हर पीर अपने काम को आगे जारी रखने के लिए अपना एक उत्तराधिकारी या वली चुनता था। भारत में सांस्कृतिक विकास
सूफियों के संत – संगठन और उनके कुछ आचारों , जैसे तप, उपवास , प्राणायाम आदि के मूल के कुछ विद्वान बौद्ध और हिंदू यौगिक प्रभाव की प्रेरणा मानते हैं।
इस्लाम के उदय के बाद भी योगी लोग पश्चिम एशिया की यात्रा करते थे और यौगिक पुस्तक अमृत – कुंड का अनुवाद संस्कृत से फारसी में हो चुका था।
उस काल के एक प्रमुख फारसी कवि सनाइ की कविता में सूफीमत की मानवीय भावना की बहुत अच्छी अभिव्यक्ति हुई।
सूफी सिलसिलों को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है – बा – शरा , अर्थात जो इस्लामी कानून ( शरा ) का पालन करते थे , और बे – शरा , अर्थात जो शरा से बंधे हुए नहीं थे। दोनों प्रकार के सिलसिले भारत में प्रचलित थे। बे – शरा सिलसिलों का अनुशासन घुमक्कड़ संत अधिक करते थे।
बा – शरा सिलसिलों में से केवल दो को तेरहवीं और चौदहवीं सदियों में उत्तर भारत में यथेष्ठ प्रभाव और बड़ी संख्या में अनुगामी प्राप्त हुए। ये थे चिश्ती और सुरावर्दी सिलसिले।
भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने की थी , जो पृथ्वीराज चौहान की पराजय और मृत्यु के कुछ दिनों बाद 1192 ईस्वी में भारत आया था। कुछ समय तक लाहौर और दिल्ली में रहने के बाद अंत में वह अजमेर चला गया। भारत में सांस्कृतिक विकास
शेख मुईनुद्दीन ( मृत्यु : 1235 ई ) के मुरीदों में बख्तियार काकी और काकी का मुरीद फरीदुद्दीन गंज – ए – शकर शामिल थे।
फरीदुद्दीन की गतिविधियों के केंद्र हांसी और अजोधन ( क्रमशः आधुनिक हरियाणा और पंजाब ) थे। उसके कुछ छंदों को सिखों के आदि – ग्रंथ में भी शामिल कर लिया गया।
चिश्ती संतों में सबसे प्रसिद्ध निजामुद्दीन औलिया और नासिरुद्दीन चिराग – ए – देहली थे। धर्मांतरण में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी , यद्यपि बाद में अनेक परिवारों और समूहों ने अपने धर्मांतरण को इन संतों की ” शुभेच्छाओं से प्रेरित ” बताया। इन संतों ने गायन के जरिए , जिसे ” समा ” कहा जाता था , लोकप्रियता अर्जित की।
निजामुद्दीन औलिया यौगिक प्राणायाम भी करता था और इसमें वह इतना पारंगत था कि योगी लोग इसे ” सिद्ध पुरुष ” कहा करते थे।
सुहरवर्दियों ने भारत में लगभग उसी समय प्रवेश किया था जब चिश्तियों ने किया था , परंतु उनकी गतिविधियां मुख्य रूप से पंजाब और मुल्तान तक सीमित थी। इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत शेख शिहाबुद्दीन सुहरवर्दी और हमीद्दीन नागौरी थे।
चिश्तियों के विपरीत सुहरवर्दी संत गरीबी का जीवन बिताने में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने राज्य की सेवा स्वीकार की और उनमें से कुछ लोग मजहबी विभाग में ऊंचे पदों पर भी थे।
दूसरी ओर चिश्ती संत राज्य की राजनीति से अलग रहना ही पसंद करते थे और शाहों तथा अमीरों की संगति से दूर रहते थे। भारत में सांस्कृतिक विकास
भक्ति आंदोलन
ईश्वर और जीव की रहस्यवादी एकता पर जोर देने वाला भक्ति आंदोलन भारत में तुर्कों के आगमन के बहुत पहले से ही काम कर रहा था।
साकार या सगुण ईश्वर की भक्ति की कल्पना का विकास बौद्ध धर्म की बढ़ती लोकप्रियता के साथ हुआ।
ईस्वी सन की प्रारंभिक सदियों के दौरान महायान बौद्ध मत में बुद्ध की पूजा अवलोकित या कृपालु के रूप में की जाने लगी। लगभग इसी समय विष्णु की उपासना का भी विकास हुआ।
गुप्त काल में रामायण और महाभारत जैसे बहुत से धर्म ग्रंथो का पुनर्लेखन किया गया तथा ज्ञान और कर्म के साथ भक्ति को भी मोक्ष के मान्य मार्ग के रूप में स्वीकार किया गया।
भक्ति का असली विकास सातवीं और बारहवीं सदियों के बीच दक्षिण भारत में हुआ। शैव नयनारों तथा वैष्णव अलवारों ने बौद्ध और जैन धर्मों की तपश्चर्या की शिक्षा को अस्वीकार करके मोक्ष के मार्ग के रूप में ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति का उपदेश दिया।
उन्होंने जाति – प्रथा को अस्वीकार कर दिया और स्थानीय भाषाओं का उपयोग करके ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम तथा भक्ति का संदेश दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में फैलाय। भारत में सांस्कृतिक विकास
भक्ति के विचारों को उत्तर ले जाने का काम विद्वानों और संतों दोनों ने किया। इनमे महाराष्ट्रीय संत नामदेव के नाम का उल्लेख किया जा सकता है जिसका जीवनकाल चौदहवीं सदी का पूर्वार्ध था।
इसी तरह इस सिलसिले में हम रामानंद का भी नाम ले सकते है जिनका जीवन – काल चौदहवीं सदी का उत्तरार्ध और पंद्रहवीं सदी का प्रथम चरण था।
नामदेव दर्जी थे जो संत बनने से पहले लुटेरे का जीवन बिताता था। मराठी में लिखी उनकी कविताएं ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति से ओत – प्रोत है। कहते हैं , नामदेव का दिल्ली में सूफी संतों के साथ संलाप भी हुआ था।
रामानुज ने अनुगामी रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था और उसने प्रयाग के अलावा काशीवास भी किया था। उसने विष्णु के स्थान पर राम की उपासना का प्रवर्तन किया।
इसे भी बड़ी बात यह थी कि रामानंद ने भक्ति का उपदेश चारों वर्णों के लोगों को दिया और विभिन्न जातियों के लोगों के एक रसोई घर में अपना खाना पकाने के साथ बैठकर खाने पर लगे निषेध को मानने से इनकार कर दिया। भारत में सांस्कृतिक विकास
रामानंद ने सभी जातियों के लोगों को अपने शिष्य बनाया। उसके शिष्यों में रविदास , कबीर , सेना और सघन भी शामिल थे। इनमें से पहला चमार , दूसरा जुलाहा , तीसरा नाई और चौथा कसाई था। नामदेव ने भी अपने शिष्य बनने में ऐसी ही उदारता का परिचय दिया।
सूफी संतों ने इस्लाम में समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांत का प्रचार किया।
जो लोग तत्कालीन समाज – व्यवस्था के सबसे प्रबल आलोचक थे और जिन्होंने हिंदू – मुस्लिम एकता की जोरदार हिमायत की उनमें कबीर और नानक के नाम अग्रणीय है।
कबीर से संबंधित कथा यह है कि वह एक विधवा ब्राह्मणी का पुत्र था जिसने जन्म होते ही उसका त्याग कर दिया और उसका लालन- पालन एक जुलाहे ने किया।
कबीर का जीवन – काल आम तौर पर पंद्रहवीं सदी माना जाता है। उसने ईश्वर के एकत्व पर जोर दिया और उसे अनेक नामों से संबोधित किया।
कबीर ने मूर्ति – पूजा , तीर्थ – व्रत , गंगादि – स्नान , नमाज और अजान , सब पर तीव्र प्रहार किया। संत जीवन जीने के लिए वह गार्हस्थ्य जीवन के त्याग को जरूरी नहीं मानता था।
कबीर सच्चे ज्ञान के लिए न तो संन्यास को जरूरी मानता था और न किताबी ज्ञान को। मनुष्य की मूलभूत एकता पर बल देते हुए उसने मानव जाति के बीच धर्म या जाति , नस्ल या परिवार अथवा संपत्ति के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव का प्रबल विरोध किया। भारत में सांस्कृतिक विकास
सिख धर्म की शिक्षाओं के स्रोत गुरु नानक का जन्म 1489 ईस्वी में रावी तट पर तलवंडी ( अब नानकाना ) नामक गांव में एक खत्री परिवार में हुआ था।
नानक ने भजनों की रचना की जिन्हें वे रबाव नामक साज के साथ गाते थे। उनका सेवक मर्दाना उनके साथ रबाव पर संगत करता था।
कहते हैं , नानक ने भारत में दूर-दूर तक यात्रा की , बल्कि वह भारत से बाहर श्रीलंका और मक्का और मदीना भी पहुंचे।
1538 ईस्वी में जब नानक की मृत्यु हुई तब तक उनकी ख्याति दूर – दूर तक फैल चुकी थी।
कबीर की तरह नानक ने भी इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर एक है और उसके नाम का जाप करने तथा उसमें लौ लगाने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है , चाहे वह किसी जाति , धर्म या पंथ का हो , परंतु नानक ने चरित्र और आचरण की शुद्धता को ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने की पहली शर्त बता कर उस पर विशेष बल दिया।
नानक ने मार्गदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता पर भी जोर दिया। कबीर की तरह नानक ने भी मूर्ति – पूजा , तीर्थ यात्राओं और विभिन्न धर्मो के अन्य औपचारिक विधि – विधानों की कड़ी आलोचना की उन्होंने मध्य मार्ग की हिमायत की। भारत में सांस्कृतिक विकास
नाना का इरादा किसी नए धर्म की स्थापना करने का नहीं था। उनके उदार दृष्टिकोण का उद्देश्य मुसलमान और हिंदुओं के बीच की खाई को पाटना था ताकि शांति , सद्भावना और पारस्परिक आदान-प्रदान का वातावरण तैयार हो सके। कबीर का उद्देश्य भी यही था।
कालांतर में नानक के विचारों ने एक नए धर्म को जन्म दिया। यह था – सिख धर्म। कबीर के अनुयायी कबीर पंथियों तक सीमित रह गए।
अकबर के धार्मिक विचारों और नीतियों में इन दो महान संतों की बुनियादी शिक्षाओं के काफी तत्व समय हुए थे। भारत में सांस्कृतिक विकास
वैष्णव आंदोलन
उत्तर भारत में विष्णु के दो अवतारों , राम और कृष्ण की उपासना को केंद्र बना कर भक्ति आंदोलन का विकास हुआ।
आरंभिक सूफियों की तरह चैतन्य ने संगीत गोष्ठी या ईश्वर नाम के कीर्तन को लोकप्रिय बनाया। चैतन्य के अनुसार उपासना प्रेम और भक्ति एवं नृत्य और संगीत में निहित थी।
गुजरात में नरसी मेहता , राजस्थान में मीरा , पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूरदास , बंगाल और उड़ीसा में चैतन्य के काव्यों के गीतात्मक माधुर्य एवं प्रेमातिरेक ने सारी सीमाओं को तोड़ डाला।
चैतन्य जी का जन्म नदिया जिले में हुआ था और उनकी आरंभिक शिक्षा भी वही हुई थी। वह ईश्वरोन्माद से ग्रस्त भक्ति के रूप में निरंतर कृष्ण नाम के कीर्तन में लीन रहते थे।
कहते हैं , चैतन्य जी ने पूरे भारत की यात्रा की थी और वह वृंदावन भी गये थे लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश समय गया में व्यतीत किया। बड़ी संख्या में लोग उनके अनुयायी बन गए। इनमें कुछ मुसलमान और नीची जातियों के हिंदू भी शामिल थे।
चैतन्य जी ने हिंदू धर्म – ग्रंथो या मूर्तिपूजा का विरोध नहीं किया। यधपि उन्हें परंपरावादी नहीं कहा जा सकता। भारत में सांस्कृतिक विकास
वेदांत दर्शन का प्रतिपादन कई विचारकों ने किया था , लेकिन जिस व्यक्ति ने संत कवियों को शायद सबसे अधिक प्रभावित किया वह था – वल्ल्भ।
वल्लभ तेलंग ब्राह्मण था और उसका जीवन – काल पंद्रहवीं सदी का अंतिम और सोलहवीं सदी का प्रारंभिक हिस्सा माना जाता है।
पंद्रहवीं सदी में महान अरब दार्शनिक इब्न – ए – अरबी के अद्वेतात्मक विचारों को भारत में बहुत बड़े वर्ग के बीच लोकप्रियता मिली।
अरबी की मान्यता थी कि सभी जीव तत्वत: एक हैं और सब कुछ एक ही परमतत्व की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार , अरबी की राय में सभी धर्म समान थे। भारत में सांस्कृतिक विकास
जीवमात्र की एकता का अरबी का सिद्धांत तौहीद – ए – वजूदी के नाम से विख्यात है। भारत में यह सिद्धांत सूफी चिंतन का मुख्य आधार बन गया।
भारतीय सूफियों ने संस्कृत और हिंदी में अधिक रुचि लेना शुरू किया और उनमें से कुछ ने , जैसे मलिक मुहम्मद जायसी ने , अपनी कृति की रचना हिंदी की अवधी बोली में की।
हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में लिखे वैष्णव भजन सूफियों के हृदय – तंतुओं का स्पर्श फ़ारसी कविता से कहीं अधिक करते थे।
हिंदी भजनों का प्रयोग उनमें इतना लोकप्रिय हो गया था कि अब्दुल वहीद बेलग्रामी नामक एक प्रसिद्ध सूफी विचारक ने हकैक – ए – हिंद शीर्षक से एक पुस्तक लिख डाली जिसमें उसने सूफी रहस्यवादी संदर्भ में कृष्ण , मुरली , गोपी , राधा , यमुना आदि शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश की। भारत में सांस्कृतिक विकास
संस्कृत साहित्य
महान शंकर के बाद रामानुज , मध्व , वल्लभ आदि ने अद्वैत दर्शन पर अपनी रचनाएं संस्कृत में ही लिखीं।
देश के अलग-अलग हिस्सों में , जिनमें मुसलमानों के शासन वाले हिस्से भी शामिल थे , संस्कृत की पीठों और विद्यालयों का एक जाल – सा बिछा हुआ था। इनमें नए शासको ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया और ये अपना काम पूर्ववत करते रहे।
बारहवीं और सोलहवीं सदियों के बीच धर्मशास्त्रों पर बड़ी संख्या में टिकाएं लिखी गई और उनके सार – संकलन तैयार किए गए।
विज्ञानेश्वर की महान कृति मिताक्षरा को , जो हिंदू कानून की दो प्रमुख धाराओं में से एक है , बारहवीं सदी से पहले की रचना नहीं माना जा सकता। एक अन्य प्रसिद्ध भाष्यकार बिहार का चण्डेश्वर था जिसका जीवन – काल चौदहवी सदी था।
जैनों ने भी संस्कृत साहित्य के विकास में योगदान किया। इनमें से सबसे प्रसिद्ध हेमचंद्र सूरी नाम का विद्वान था।
इस्लामी कृतियों या फारसी साहित्य का संस्कृत में अनुवाद करने की कोई कोशिश नहीं की गई। इसका शायद एकमात्र अपवाद प्रसिद्ध फारसी कवि जामी की लिखी यूसुफ और जुलेखा की प्रेमकथा थी। भारत में सांस्कृतिक विकास
अरबी और फ़ारसी साहित्य
यद्यपि मुसलमानों द्वारा लिखा सबसे अधिक साहित्य अरबी में था। यद्यपि भारत आने वाले तुर्कों पर फारसी का गहरा प्रभाव था और यह भाषा दसवीं सदी से मध्य एशिया की साहित्य और प्रशासन की भाषा बन गई थी।
कालांतर में भारतीय विद्वानों की सहायता से इस्लामी कानून के सार – संकलन फारसी में तैयार करवाए गए। इनमें से सबसे प्रसिद्ध संकलन फिरोज तुगलक के शासनकाल में तैयार किए गए।
अरबी सार – संकलन भी तैयार किए जाते रहे। इनमे सबसे प्रसिद्ध फतवा – ए – आलमगीरी अर्थात औरंगजेब के शासनकाल में विधिवेत्ताओं के एक समूह द्वारा तैयार किया गया कानूनों का सार – संकलन है।
दसवीं सदी में तुर्कों के भारत आगमन के साथ इस देश में एक नई भाषा अर्थात फ़ारसी का प्रवेश हुआ। फारसी के कुछ महानतम कवि जैसे – फिरदोसी और सादी का जीवनकाल दसवीं से चौदहवीं सदी के बीच पड़ता है।
फ़ारसी के प्रारंभिक भारतीय लेखकों में से कुछ की ही कृतियां शेष बची है। इनमें से दो-चार ऐसे हैं – जैसे कि मसूद साद सलमान – जिसके लेखन में हमें लाहौर के प्रति लगाव और प्रेम की भावना की झलक मिलती है। भारत में सांस्कृतिक विकास
इस दौर का सबसे उल्लेखनीय फारसी लेखक अमीर खुसरो था। 1252 ईस्वी में पटियाला ( पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बदायूं जिला ) में जन्मे अमीर खुसरो को भारतीय होने पर गर्व था।
अमीर खुसरो कहता है – ” मैंने भारत की प्रशंसा दो कारणों से ही है। एक तो यह है कि हिंदुस्तान मेरी जन्म भूमि और हम सबका वतन है। वतन से प्यार करना एक अहम फर्ज है।…. हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है। इसकी आबोहवा खुरासान से बेहतर है ……. यह हरा-भरा है और सालों भर फूलों से लदा रहता है ……. यहां के अरस्तू जैसे ज्ञानी ब्राह्मण है और विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे विद्वान है “।
खुसरो ने फ़ारसी की एक नई शैली की सृष्टि की , जो सबक – ए – हिंदी , अर्थात हिंदुस्तान की शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई।
खुसरो ने भारतीय भाषाओं की भी प्रशंसा की है। इनमें हिंदी भी शामिल है जिसे वह हिंदवी कहता है। भारत में सांस्कृतिक विकास
खुसरो को खालिक बारी की रचना का भी श्रेय दिया जाता है , लेकिन मालूम होता है , वह इसी नाम के कवि की कृति थी।
खुसरो एक कुशल संगीतज्ञ भी था , और वह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की धार्मिक संगीत गोष्ठियों में भाग लेता था।
कहते हैं , जिस दिन उसने अपने पीर निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु ( 1325 ई ) का समाचार सुना उसके अगले ही दिन उसने भी शरीर – त्याग कर दिया और उसे उसी अहाते में दफन किया गया जिसमें निजामुद्दीन औलिया को दफन किया गया था।
इस काल में फारसी में इतिहास – लेखन की एक प्रबल शैली उभरी। जियाउद्दीन बरनी , अफ्रीका और इसामी इस काल के सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार थे।
फ़ारसी के माध्यम से भारत ने मध्य एशिया तथा ईरान के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए।
संस्कृत और फारसी ने राजनीति , धर्म और दर्शन के क्षेत्रों में देश के लिए संपर्क भाषाओं का काम किया। और साथ ही वे साहित्यिक कृतियों की भी भाषाएं थी।
जिया नक्शबी ( 1350 ई ) पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया। ये कथाएँ एक स्त्री को , जिसका पति लंबी यात्रा पर गया हुआ है , तोते के मुंह से कहलवाई गई हैं। भारत में सांस्कृतिक विकास
फिरोज तुगलक के शासनकाल में लिखी फारसी की यह रचना ‘ तूतीनामा ‘ बहुत लोकप्रिय हुई थी। इसका अनुवाद फारसी से तुर्क भाषा में और यूरोपीय भाषाओं में भी किया गया।
नक्शबी ने कामशास्त्र पर प्राचीन भारतीय रचना कोकशास्त्र का भी फारसी में अनुवाद किया।
फिरोज शाह के ही शासनकाल में आयुर्विज्ञान तथा संगीत पर संस्कृत रचनाओं का अनुवाद फारसी में किया गया।
कश्मीर के सुल्तान जैन – उल – आबिदीन ने प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति राजतरंगिणी और महाभारत का अनुवाद संस्कृत से फारसी में करवाया। उसके निर्देश पर आयुर्विज्ञान तथा संगीत पर भी संस्कृत कृतियों का फारसी में अनुवाद किया गया। भारत में सांस्कृतिक विकास
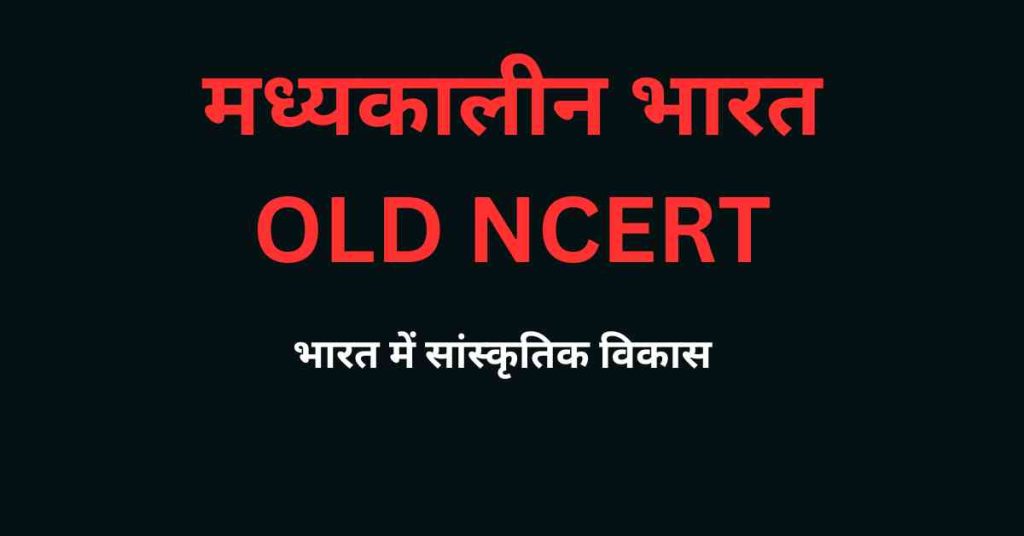
क्षेत्रीय भाषाएँ
इस काल में कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी उच्च कोटि के साहित्य की रचनाएँ की गई।
चौदहवीं सदी के आरंभ में लिखते हुए अमीर खुसरो ने क्षेत्रीय भाषाओं के अस्तित्व का उल्लेख किया है।
क्षेत्रीय भाषाओं का परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करना और साहित्यिक कृतियों के लिए इनका उपयोग मध्यकाल की एक उल्लेखनीय विशेषता माना जा सकता है।
भक्त संतों द्वारा आम लोगों की भाषा का प्रयोग , निस्संदेह , क्षेत्रीय भाषाओं के उत्थान का एक बहुत बड़ा कारण था।
तुर्कों के शासन की स्थापना के पूर्व कई क्षेत्रीय राज्यों में संस्कृत के अलावा तमिल, कन्नड़ , मराठी आदि क्षेत्रीय भाषाएं प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। यह परंपरा तुर्क शासन के अधीन भी जारी रही। भारत में सांस्कृतिक विकास
दक्षिण भारत में तेलुगु में साहित्य का विकास विजयनगर राज्य के संरक्षण में हुआ।
मराठी बहमनी सल्तनत की एक प्रशासनिक भाषा थी और बाद में बीजापुर दरबार की भी भाषा यही रही।
बंगाल के नुसरत शाह ने महाभारत और रामायण का बंगला में अनुवाद करवाया। उसी के संरक्षण में मालाधर बसु भागवत का भी बंगला में अनुवाद किया।
जौनपुर में मलिक मुहम्मद जायसी जैसे सूफी संतों ने अपनी रचनाएं अवधी में लिखी। उन्होंने मसनवी आदि कई फारसी शैलियों को लोकप्रिय बनाया। भारत में सांस्कृतिक विकास
ललित कलाएँ
तुर्क लोग अपने साथ रबाब और सारंगी जैसे कई वाद्य यंत्र तथा नई संगीत पद्धतियां और नियम भी लाए थे।
खुसरो को नायक का खिताब दिया गया था। जिसका मतलब यह था कि वह संगीत के सिद्धांत और उसके व्यावहारिक प्रयोग में भी पारंगत था।
खुसरो ने फारसी अरबी मूल के कई राग जैसे एमन , घोर आदि , भारतीय संगीत में दाखिल किए। उसे सितार को ईजाद करने का श्रेय भी दिया जाता है यद्यपि इसके समर्थन में हमें कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
तबले का आविष्कार का श्रेय भी खुसरो को दिया जाता है , लेकिन जान पड़ता है कि उसका विकास सत्रहवीं के अंत या अठारहवीं सदी के आरंभ में हुआ।
फिरोज के शासनकाल में संगीत पर मानक भारतीय ग्रंथ ‘ रागदर्पण ‘ का फारसी में अनुवाद किया गया। जौनपुर का सुल्तान हुसैन शर्की संगीत का महान संरक्षक था।
सूफी संत पीर बोधन को उस काल का दूसरा महान संगीतज्ञ माना जाता है।
ग्वालियर का राजा मानसिंह बहुत बड़ा संगीत प्रेमी था। मान कौतूहल , जिसमें मुसलमानों द्वारा भारतीय संगीत में दाखिल की गई सभी पद्धतियों का वर्णन है , उसी के तत्वावधान में तैयार किया गया था।
कश्मीर राज्य में फारसी संगीत से भरपूर तौर पर प्रभावित एक विशिष्ट संगीत शैली का विकास हुआ। भारत में सांस्कृतिक विकास
Short Questions And Answers
प्रश्न 1 – कुतुब मीनार के निकट कुव्वल – उल – इस्लाम मस्जिद मूलतः क्या था ?
उत्तर – एक जैन मंदिर।
प्रश्न 2 – मेहराबों और गुंबदों का ईजाद किया था :-
उत्तर – रोमनों ने।
प्रश्न 3 – तुर्क शासकों ने किस वास्तुकला पद्धति का उपयोग किया ?
उत्तर – गुंबद-मेहराब और लिंटल-शहतीर पद्धति।
प्रश्न 4 – तुर्कों ने सजावट में किसका इस्तेमाल किया ?
उत्तर – ज्यामितीय और पुष्प डिज़ाइन, कुरान की आयतों, और हिन्दू प्रतीकों का।
प्रश्न 5 – तुर्क इमारतों में कौन से पत्थरों का उपयोग किया गया ?
उत्तर – लाल, सफेद, और पीले बलुई पत्थरों तथा संगमरमर का।
प्रश्न 6 – सजावटी युक्तियों के संयोग को क्या कहा जाता था ?
उत्तर – अरेबेस्क
प्रश्न 7 – कुतुबमीनार का निर्माण क्यों और कब हुआ ?
उत्तर – यह 13वीं सदी में सूफी संत कुतुबमीनार बख्तियार काकी की स्मृति में बना।
प्रश्न 8 – अलाउद्दीन द्वारा कुतुबमीनार में जोड़ गए प्रवेश द्वार का क्या नाम है ?
उत्तर – अलाई दरवाजा।
प्रश्न 9 – वैज्ञानिक पद्धति से बनाया गया सही पहला गुंबद है –
उत्तर – अलाई दरवाजे में।
प्रश्न 10 – तुगलक काल में भवन निर्माण में क्या बदलाव हुआ ?
उत्तर – भवन निर्माण की गतिविधियों में तेजी आई।
प्रश्न 11 – तुगलक स्थापत्य की प्रमुख विशेषता क्या थी?
उत्तर – ढालू दीवारें, जो मजबूती और ठोसपन का एहसास कराती थीं।
प्रश्न 12 – तुगलक स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता ढालू दीवार है , लेकिन किस तुगलक शासक की इमारतों में हमें ढालू दीवारें देखने को नहीं मिलती ?
उत्तर – फिरोज तुगलक।
प्रश्न 13 – तुगलक इमारतों में किस प्रकार के पत्थरों का उपयोग किया गया ?
उत्तर – सस्ते और आसानी से उपलब्ध भूरे पत्थरों का।
प्रश्न 14 – लोदी कालीन स्थापत्य की विशेषता क्या थी ?
उत्तर – ऊंचे चबूतरों पर मकबरे, छज्जे, छतरियां, और अष्टभुजाकार मकबरे।
प्रश्न 15 – सूफी आंदोलन भारत में कब प्रभावी हुआ ?
उत्तर – 12वीं सदी के बाद।
प्रश्न 16 – इस्लामी कानून की चार धाराओं में से सबसे उदार धारा कौन सी थी ?
उत्तर – हनीफी।
प्रश्न 17 – हर सूफी सिलसिलें का नेतृत्व आम तौर पर एक प्रसिद्ध सूफी संत करता था जो कहलाता था –
उत्तर – पीर।
प्रश्न 18 – हर पीर अपने काम को आगे जारी रखने के लिए अपना एक उत्तराधिकारी चुनता था , उसे क्या कहते थे ?
उत्तर – वली।
प्रश्न 19 – सूफी सिलसिलों को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है –
उत्तर – बा-शरा ( इस्लामी कानून का पालन ) और बे-शरा ( इस्लामी कानून से मुक्त ) ।
प्रश्न 20 – भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की?
उत्तर – ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती।
प्रश्न 21 – बख्तियार काकी और काकी का मुरीद फरीदुद्दीन गंज – ए – शकर किसके मुरीद थे ?
उत्तर – शेख मुईनुद्दीन।
प्रश्न 22 – किस सूफी के कुछ छंदों को सिखों के आदि – ग्रंथ में भी शामिल कर लिया गया ?
उत्तर – फरीदुद्दीन।
प्रश्न 23 – निजामुद्दीन औलिया यौगिक प्राणायाम करता था और इसमें वह इतना पारंगत था कि योगी लोग इसे कहा करते थे –
उत्तर – सिद्ध पुरुष।
प्रश्न 24 – भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक विकास कहाँ हुआ ?
उत्तर – दक्षिण भारत में, 7वीं और 12वीं सदी के बीच।
प्रश्न 25 – सिख धर्म की शिक्षाओं के स्रोत गुरु नानक का जन्म 1489 ईस्वी में हुआ था –
उत्तर – रावी तट पर तलवंडी ( अब नानकाना ) नामक गांव में एक खत्री परिवार में।
प्रश्न 26 – नानक ने अपने भजनों के लिए कौन सा वाद्ययंत्र उपयोग किया ?
उत्तर – रबाब।
प्रश्न 27 – गुरु नानक के विचारो ने जिस नए धर्म को जन्म दिया , वह है –
उत्तर – सिख धर्म।
प्रश्न 28 – कबीर के अनुयायी कहलाते है ?
उत्तर – कबीर पंथी।
प्रश्न 29 – उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का केंद्र कौन-से दो अवतार बने ?
उत्तर – राम और कृष्ण।
प्रश्न 30 – चैतन्य जी का जन्म और शिक्षा कहाँ हुई थी ?
उत्तर – नदिया जिले में।
प्रश्न 31 – जीवमात्र की एकता का अरबी का सिद्धांत विख्यात है –
उत्तर – तौहीद – ए – वजूदी के नाम से।
प्रश्न 32 – इब्न-ए-अरबी का सिद्धांत क्या था ?
उत्तर – जीवमात्र की एकता और सभी धर्मों की समानता।
प्रश्न 33 – भारतीय सूफियों ने किस भाषा में अधिक रुचि ली ?
उत्तर – संस्कृत और हिंदी।
प्रश्न 34 – मलिक मुहम्मद जायसी ने किस भाषा में रचनाएँ कीं ?
उत्तर – हिंदी की अवधी बोली।
प्रश्न 35 – हकैक – ए – हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे ?
उत्तर – अब्दुल वहीद बेलग्रामी।
प्रश्न 36 – रामानुज , मध्व , वल्लभ आदि ने अद्वैत दर्शन पर अपनी रचनाएं किस भाषा में लिखीं ?
उत्तर – संस्कृत में।
प्रश्न 37 – धर्मशास्त्रों पर बड़ी संख्या में टिकाएं कब लिखी गईं ?
उत्तर – बारहवीं और सोलहवीं सदियों के बीच।
प्रश्न 38 – हिंदू कानून की दो प्रमुख धाराओं में से एक मिताक्षरा किसकी रचना है ?
उत्तर – विज्ञानेश्वर।
प्रश्न 39 – भारत में फारसी भाषा का प्रवेश कब हुआ ?
उत्तर – दसवीं सदी में तुर्कों के आगमन के साथ।
प्रश्न 40 – खुसरो की फारसी शैली का नाम क्या था ?
उत्तर – सबक-ए-हिंदी।
प्रश्न 41 – वह पहला व्यक्ति कौन था , जिसने संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया ?
उत्तर – जिया नक्शबी ( 1350 ई )।
प्रश्न 42 – फारसी की रचना ‘ तूतीनामा ‘ के लेखक कौन थे ?
उत्तर – जिया नक्शबी।
प्रश्न 43 – क्षेत्रीय भाषाओं का परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करना और साहित्यिक कृतियों के लिए इनका उपयोग किस काल की एक उल्लेखनीय विशेषता माना जा सकता है ?
उत्तर – मध्यकाल।
प्रश्न 44 – दक्षिण भारत में तेलुगु में साहित्य का विकास किस राज्य के संरक्षण में हुआ ?
उत्तर – विजयनगर।
प्रश्न 45 – किसने फारसी अरबी मूल के कई राग जैसे एमन , घोर आदि , भारतीय संगीत में दाखिल किए ?
उत्तर – खुसरो ने।
प्रश्न 46 – सितार और तबले का आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है ?
उत्तर – अमीर खुसरो।